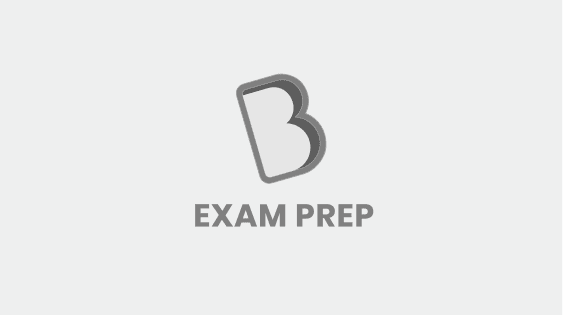- Home/
- Bihar State Exams (BPSC)/
- Article
न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023

भारत में संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक के रूप में सत्ता का पृथक्करण है जहां विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के डोमेन की अपनी भूमिका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के संरक्षक होने की जिम्मेदारी के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली को स्वतंत्र (हालांकि एकीकृत) के रूप में परिकल्पित किया। लेकिन कुछ मामलों में न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में अपनी विशाल शक्ति का प्रदर्शन करती है। इस लेख में हम न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे।
Table of content
न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक संयम
न्यायिक सक्रियता का अर्थ
- नागरिकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई अतिसक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है।
- यह एक न्यायिक धारणा है जिसमें न्यायपालिका बड़े पैमाने पर समाज के लोगों के लिए लाभकारी संवैधानिक रूप से सही कानूनों को लागू करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है।
- न्यायिक सक्रियता में, न्यायपालिका अपनी शक्ति का उपयोग उन कानूनों या नियमों को रद्द करने के लिए करती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों में बाधा उत्पन्न करते हैं या संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल होते हैं।
- यह न्यायपालिका को सरकार की अन्य संस्थाओं/शाखाओं की गलतियों या अन्याय को ठीक करने का अधिकार प्रदान करता है।
- गोलक नाथ केस (1967), केशवानंद भारती केस (1973), मेनका केस (1973), विशाखा केस (1997) आदि में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले न्यायिक सक्रियता के कुछ उदाहरण हैं।
न्यायिक संयम का अर्थ
- वह सिद्धांत, जिसमें न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी कानून या नियम को रोकने के लिए तब तक संयम रखती है जब तक कि वह देश के संवैधानिक मूल्यों के पूर्णत: विरुद्ध न हो, न्यायिक संयम कहलाता है।
- न्यायिक संयम इस तथ्य पर विचार करते हुए न्यायपालिका को प्रोत्साहित करता है कि संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित कानून/नियम समय की आवश्यकता हो सकते हैं और न्यायपालिका द्वारा आवश्यकता का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि संविधान की रक्षा के लिए इसे रोकने की जरूरत न हो।
महत्वपूर्ण तथ्य
- संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को उन सभी कानून/अधिनियम/नियम की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है जो देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- किसी भी कानून/अधिनियम/नियम की समीक्षा करने का न्यायपालिका का यह अधिकार प्रबल हो गया और बाद के वर्षों में इसे न्यायिक सक्रियता कहा गया। हालांकि, संविधान में ‘न्यायिक सक्रियता’ शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है।
- न्यायिक सक्रियता भारतीय न्यायपालिका का आविष्कार है, जो जनहित याचिका (PIL) या अन्य किसी माध्यम से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करके सक्रिय निर्णय देता है।
- न्यायिक सक्रियता का सफर गोलक नाथ केस (1967) से शुरू हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के भाग- III में दिए गए मौलिक अधिकार विधायिका द्वारा संशोधित के योग्य नहीं हैं।
- केशवानंद भारती केस (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की ‘मूल संरचना’ की अवधारणा प्रस्तुत करके एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि संविधान की ‘मूल संरचना’ को परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- एस.पी. गुप्ता केस (1981) में, जनहित याचिका की एक नई अवधारणा पेश की गई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार किया गया।
- यहां से, सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के मुद्दों में भी अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का उपयोग अधिक बेतरतीब ढंग से करना शुरू कर दिया।
न्यायिक सक्रियता के हाल ही के मुकदमे
- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया। बाद में निर्णय में संशोधन किया गया और इसे वैकल्पिक बना दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्जुन गोपाल केस में, दिल्ली/NCR में पर्यावरण के प्रतिकूल पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और यहां तक कि पटाखे फोड़ने का समय भी निर्धारित किया।
- सुभाष काशीनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में संशोधन करने की घोषणा की।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने हाल ही में 15-वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और 10-वर्ष पुराने डीजल वाहन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
- तमिलनाडु के एक न्यायाधीश ने तमिलनाडु के प्रत्येक छात्र के लिए तिरुक्कुरल के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया, जो वास्तव में विधायिका और कार्यपालिका का विशेषाधिकार है।
- ऐसे कईं अन्य निर्णय हैं, जिनमें न्यायाधीशों ने शक्तियों का अत्यधिक उपयोग किया है और विधायिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया।
न्यायिक सक्रियता के क्रमिक विकास के कारण
- कानून की विफलता – कईं संवेदनशील मामलों में, जब मौजूदा कानून मामले को संभालने में विफल हो जाते हैं, न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। जैसे – सर्वोच्च न्यायालय का तीन तलाक मामले पर निर्णय।
- पिछले फैसलों की समीक्षा – कईं मामलों में, परिस्थिति न्यायालय को अपने पहले के फैसलों पर एक नई मनोदशा के साथ विचार करने की मांग करती है। ऐसी स्थिति में भी न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सहायता करती है।
- न्यायिक शून्यता को भरना – कईं बार, सर्वोच्च न्यायालय को एक समान घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्वप्रेरणा से कार्य करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दों से निपटने के लिए वर्ष 1997 के विशाखा मामले से विशाखा दिशा-निर्देश तैयार किए।
- चेक और शेष राशि के लिए – कईं बार, सत्ता में सरकार शीघ्रता में निर्णय लेती है और ऐसे मामलों में, न्यायालय संविधान के अनुसार कानून/अधिनियम की वैधता की जांच करते हैं।
- समय पर और पूर्ण निर्णय के लिए – कईं बार, परिस्थिति के अनुसार समय पर और पूर्ण न्याय के लिए न्यायालयों की सक्रिय प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। ऐसे मामलों में, न्यायालय कानून लागू करने के अधिकार का उपयोग कर सकता है।
- मानवाधिकारों की बढ़ती मांग – दुनिया भर में और भारत में भी मानवाधिकारों की प्रधानता सिद्ध करने की नियमित मांग की गई है। इसने न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की अपनी शक्ति के अंतर्गत आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।
न्यायिक स्वतंत्रता
- संविधान ने अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों और शक्तियों को अलग कर दिया है।
- संविधान का अनुच्छेद 121 और 211 न्यायाधीशों द्वारा दायित्व निर्वाह करते हुए उनके आचरण पर बहस करने से विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल, नियुक्ति, वेतन और भत्ते आदि की सुरक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- न्यायाधीशों को विधायिका और कार्यपालिका से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता से निर्वहन करने की स्वतंत्रता है।
- न्यायालयों के आदेश पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति या विरोध नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम और अनिवार्य होता है और इसे केवल परस्पर उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।
न्यायिक सक्रियता के दोष
- न्यायपालिका की अधिभावी शक्तियों ने कई बार विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दिया है, जो संविधान में निहित शक्तियों के वियोजन की भावना के विपरीत है।
- कई बार, न्यायाधीशों के व्यक्तिगत और पूर्वाग्रहित विचार उनके निर्णयों में दिखाई देते हैं, जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की सबसे बड़ी कमी है।
- एक फैसला अन्य मामलों के लिए आदर्श फैसला बन जाता है जिसके फलस्वरूप न्यायिक ठगी की एक श्रृंखला बन जाती है।
- न्यायिक सक्रियता संसद और विधायिका की कानून बनाने की शक्ति को परिमित करती है।
- न्यायिक सक्रियता को न्यायिक ठगी में बदलने की संभावना बहुत अधिक है और इसलिए न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे समझना जरूरी है।
- कई बार, न्यायपालिका द्वारा लिए गए फैसलों ने संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए कानून में जनता के विश्वास को खत्म किया है।
- समग्र रूप से, न्यायिक सक्रियता विधायिका की कानून बनाने की प्रक्रिया में एक चुनौती बन गई है।
भविष्य की अनिवार्यताएं
- न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता और न्यायिक ठगी के बीच के बारीक अंतर को समझना जरूरी है और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।
- न्यायपालिका को अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए शक्ति के वियोजन की अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए।
- न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना जरूरी है, और इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नए तरीके अपनाए जा सकते हैं।
- विधायिका को वैधानिक अंतराल भरने के लिए अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है ताकि न्यायिक समीक्षा और हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाए।
- न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के अंतर्गत न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिक अनुशासित और जवाबदेह होना चाहिए।
Most Important Study Notes
BPSC/CDPO के लिए Complete Free Study Notes, अभी Download करें
Download Free PDFs of Daily, Weekly & Monthly करेंट अफेयर्स in Hindi & English
NCERT Books तथा उनकी Summary की PDFs अब Free में Download करें