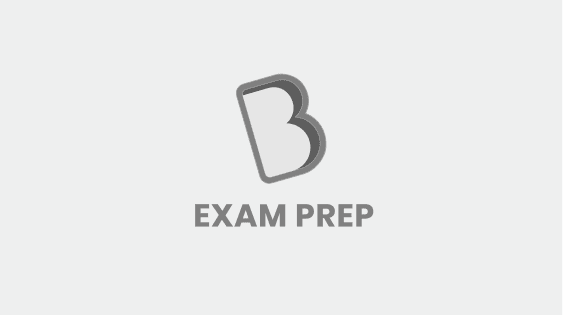स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन – एक राष्ट्र के रूप में भारत का एकीकरण
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: November 14th, 2023
स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के समय, भारत में लगभग 565 रियासतें थीं। एक विशाल देश होने के नाते, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन चुनौतीपूर्ण था। इसे सरदार पटेल के असाधारण नेतृत्व द्वारा पूरा किया गया जिन्होंने एक एकीकृत राष्ट्र के सपने को संभव बनाया।
स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया सुचारू नहीं थी। भारत सरकार और उसके नेताओं को इस प्रक्रिया में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन आखिरकार, वे विभिन्न रणनीति अपनाकर अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हुए।
Table of content
स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन
जैसे ही भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और अंग्रेजों ने देश छोड़ने का फैसला किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और मुस्लिम लीग को एकता (Unity) की चुनौती का सामना करना पड़ा। वे एक-दूसरे के साथ सहयोग करने में असफल रहे जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में, ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी क्षेत्रों के साथ 565 रियासतें थीं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन का विचार एक कठिन कार्य लगता था।
ब्रिटेन ने भी सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया और इसके लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा। चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को “डायरेक्ट एक्शन डे” के रूप में घोषित किया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोनों सीमाओं पर हिंसा हुई और अंततः कांग्रेस द्वारा विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया गया।
- 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो अलग-अलग राष्ट्रों के गठन हुआ।
- यह विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था जिसे 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था।
- पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान कहा जाता था जो कुछ वर्षों के बाद पुनः विभाजित हो गया।
- परिणामस्वरूप, 1975 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का गठन किया गया।
- एक अन्य मुद्दा जो उस समय विद्यमान था, वह रियासतों का एकीकरण था क्योंकि इनमें से कुछ राज्य स्वतंत्रता और पृथक राज्यों के रूप में रहना चाहते थे।
स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण
घोर गरीबी, अत्यधिक भुखमरी, उप-स्तरीय अर्थव्यवस्था और शरणार्थियों के पुनर्वास की बड़ी समस्याओं, स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन जैसी समस्याओं के अलावा, प्रमुख रियासतों का एकीकरण की एक बड़ी चुनौती थी। विभाजन के बाद न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी धर्म के नाम पर अपराध दर और हिंसा में वृद्धि हुई। हिंसा के कारण लगभग 80 लाख लोगों का पलायन हुआ और 10 लाख लोग मारे गए। भारत को शरणार्थियों को बसाने के लिए एक पुनर्वास विभाग बनाना पड़ा।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों के साथ-साथ 500 से अधिक रियासतें थीं और ब्रिटिश सरकार के साथ कुछ मौजूदा राजस्व व्यवस्थाएँ थीं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण कठिन था, खासकर जब 1946 और 1947 के बीच स्टेट पीपल्स मूवमेंट नाम का एक अलग विद्रोह हुआ।
- संविधान सभा में चुनावों में राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था।
- जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सत्रों की अध्यक्षता की और घोषणा की कि जो भी राज्य विधानसभा में शामिल होने से इनकार करेंगे, उन्हें विपक्ष माना जाएगा।
- सरदार पटेल ने अंततः 1947 में सचिव के रूप में वी. पी. मेनन के साथ राज्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली।
भारत का एकीकरण – चरण 1
सरदार वल्लभभाई पटेल ने मामलों को अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया में शामिल जोखिमों को समझा। स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सरदार पटेल ने दो-चरणीय दृष्टिकोण का पालन किया और सबसे पहले कुछ रियासतों के प्रमुखों से अपील की।
- भारत के भीतर आने वाले राज्यों से तीन आधारों पर भारत संघ की शर्तों को स्वीकार करने की अपील की गई थी- विदेशी मामले, संचार और रक्षा।
- सरदार पटेल ने चेतावनी भी दी कि 15 अगस्त के बाद सरकार की शर्ते और कठोर होंगी।
- उन्होंने प्रिवी पर्स (शाही भत्ता) के नाम पर आकर्षक मुआवजे के द्वारा राजकुमारों को भी लुभाया और इन राज्यों को भारत का हिस्सा बनने में दिलचस्पी थी।
- इसके परिणामस्वरूप, 562 राज्यों ने वास्तव में अधिमिलन पत्र (अंगीकार पत्र) पर सहमति व्यक्त की और हस्ताक्षर किए और तीन रियासतों अर्थात हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने इस पर सहमति नहीं जताई।
एक राष्ट्र के रूप में भारत का एकीकरण
सरदार पटेल ने रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में भारी योगदान दिया। उन्होंने रियासतों के राजकुमारों को समझाने में माउंटबेटन से भी सहायता ली। लगभग सभी राज्यों के सफल एकीकरण के बाद शेष तीन राज्यों के एकीकरण की चुनौती बची थी। इसलिए, पटेल ने निम्नलिखित तरीके से उनके एकीकरण हेतु अपने प्रयासों की शुरुआत की।
जूनागढ़ का विलय
हिन्दुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद, जूनागढ़ पर मुहम्मद महाबत खानजी तृतीय नाम के एक मुस्लिम शासक का नियंत्रण था। जूनागढ़ के शासक ने इस तथ्य के बावजूद अपने राज्य के पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी कि उसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं लगती थीं।
- उसने ऐसा अपने लोगों की इच्छा के विरुद्ध किया, जो बहुसंख्यक हिंदू थे और पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र था।
- परिणामस्वरूप, लोगों ने एक विद्रोह की योजना बनाई और नवाब को भगा दिया, जिससे एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई।
- इन सबके बाद जूनागढ़ के दीवान ने भारत सरकार से मामलों को अपने हाथों में लेने और निष्पक्ष निर्णय करने का अनुरोध किया।
- इसलिए, 1948 में जूनागढ़ में एक मतदान आयोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया।
हैदराबाद का विलय
चूँकि हैदराबाद सबसे बड़ा भारतीय राज्य था, ऐसे में भारत के साथ विलय नहीं करने का उसका निर्णय देश के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता था। हैदराबाद के नवाब स्वतंत्र दर्जा चाहते थे और अपनी सैन्य शक्ति को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें भारत के साथ एकीकरण में कम दिलचस्पी थी।
- कई चर्चाओं और वार्ताओं के बाद, भारत ने “स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट” (Standstill Agreement) नामक एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत को उम्मीद थी कि हैदराबाद के नवाब एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे लेकिन वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को धीमा कर रहे थे।
- हैदराबाद के नवाब के साथ काफी समय तक विचार-विमर्श चलता रहा।
- आखिरकार, नवाब को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को जबरदस्ती हैदराबाद में प्रवेश किया।
- हैदराबाद राज्य आखिरकार नवंबर के महीने में भारत का अंग बन गया।
कश्मीर का विलय
मुस्लिमों की संख्या अधिक होने के बावजूद, जम्मू और कश्मीर राज्य का नेतृत्व एक हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह कर रहे थे। महाराजा ने भ्रम की स्थिति पैदा की और उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ “स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट” (Standstill Agreement) हस्ताक्षर किए।
- कश्मीर के महाराजा प्रमुख रूप से एक स्वतंत्र दर्जा बनाए रखने में रुचि रखते थे।
- हालाँकि, भारत के राजनीतिक नेताओं ने कश्मीर को एकीकरण स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
- कुछ समय बाद, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने का प्रयास किया जो महाराजा के लिए एक चेतावनी थी।
- बाद में उन्होंने सैन्य सहायता के लिए भारत से अनुरोध किया और अधिमिलन पत्र (अंगीकार पत्र) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।
स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण – चरण 2
स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन के दूसरे चरण में एक कठिन कार्य शामिल था। दूसरी चुनौती भारत से सटे देशी रियासतों को प्रांतों में मिलाने की थी। ये राज्य थे नेपाल, भूटान और सिक्किम। इन राज्यों में से भूटान और नेपाल ने अंततः खुद को स्वतंत्र देशों के रूप में अलग कर लिया।
एकीकरण के परिणामस्वरूप पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU), मध्य भारत, राजस्थान, त्रावणकोर-कोचीन और सौराष्ट्र जैसे पांच संघ अब भारत का हिस्सा थे। हैदराबाद, त्रावणकोर-कोचीन और मैसूर जैसे कई राज्यों ने अपनी सीमाओं को बनाए रखने का फैसला किया।
स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन
राज्यों और अन्य ब्रिटिश प्रांतों के विलय के बाद उनकी सांस्कृतिक या भाषाई पहलुओं के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों का एक अस्थायी पुनर्गठन किया गया। चीजों को स्थिर करने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश के भीतर राज्यों के एकीकरण और पुनर्गठन के संबंध में स्थायी कार्रवाई की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कुछ आयोगों का गठन किया गया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में काम किया।
- धर आयोग – भाषाई प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के अनुरोध किए गए थे। इसके कारण 1948 में धार आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष एस.के. धर थे। आयोग भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी पुनर्गठन के पक्ष में था।
- जे. वी. पी. समिति- धर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों ने लोगों की आवश्यकताओं, विशेष रूप से दक्षिण क्षेत्र के लोगों की, को पूरा नहीं किया। इसके चलते 1948 में ही जे. वी. पी. समिति का गठन किया गया। समिति में पंडित नेहरू, पट्टाभि सीतारमैय्या और वल्लभ भाई पटेल शामिल थे जिन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने एक बार फिर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया।
- आंध्र आंदोलन 1953 – जे. वी. पी. समिति की सिफारिशों के बाद, 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बन गया। बाद में सरकार द्वारा तेलुगु भाषी लोगों को मद्रास राज्य से अलग कर दिया गया।
स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण और पुनर्गठन: नए राज्यों का गठन
भाषाई या सांस्कृतिक आधार पर नए राज्यों के गठन से संबंधित कई अनुरोध किए गए थे। इसके कारण पहले से अस्तित्व में रहे भारतीय राज्यों का विभाजन भी हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
- गुजरात और महाराष्ट्र – बॉम्बे 1960 में एक द्विभाषी राज्य था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बॉम्बे को 2 राज्यों में विभाजित किया गया- महाराष्ट्र, जिसमें मराठी बोलने वाले लोग शामिल थे और गुजरात जिसमें गुजराती बोलने वाले लोग शामिल थे।
- दमन और दीव और गोवा – ये तीनों पुर्तगाली क्षेत्रों का एक हिस्सा थे जिन्हें 1961 में सशस्त्र हमलों के माध्यम से जबरन छीन लिया गया था। तीनों एक ही क्षेत्र का हिस्सा थे, जिसमें से गोवा बाद में 1987 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग हो गया था।
- दादरा और नगर हवेली – यह भी 1954 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। बाद में 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
- पुडुचेरी – यह फ्रांसीसी क्षेत्र का एक हिस्सा था और 1954 में भारत का हिस्सा बन गया और केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
उपर्युक्त राज्यों के अलावा, अन्य नए राज्य भी थे जो भारत में राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बने थे। वे थे
- नगालैंड
- चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा
- त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय
- सिक्किम
- अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
- उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़
- तेलंगाना
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख